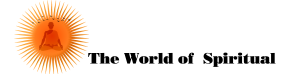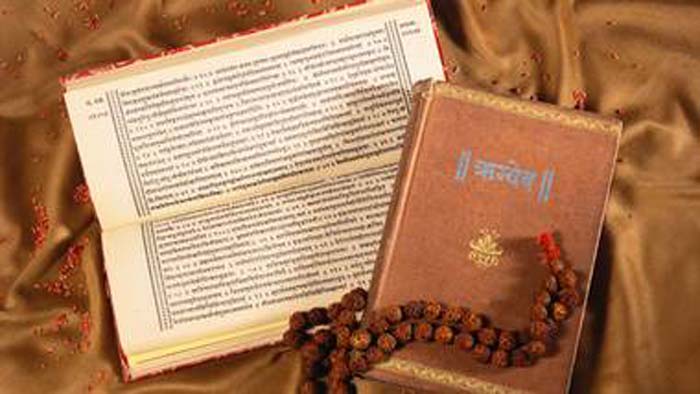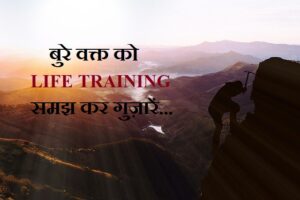वेद शब्द ‘विद्‘ धातु से आया है जिसका अर्थ होता है ‘जानना’. To know. ब्रह्म की कोई सीमा नहीं। इसलिए जानने की कोई सीमा नहीं। ज्ञान— वेद अनंत है। ऋषियों द्वारा की गयी यह अभिव्यक्ति सत्य-युग की है। सतयुग में समाज में perfection था। सभी स्वतः धर्मनिष्ठ थे। आर्य सभ्यता ह्रास यानि Devolution ( सत्ययुग से कलि युग ) की कहानी है, विकास / Evolution की नहीं। ‘विद्‘ धातु से उत्पन्न ‘वेद’ का अर्थ है जानना, ज्ञान। इसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए वेद अखण्ड हैं. जानने की कोई सीमा नहीं होती। अतः महर्षि वेदव्यास द्वारा चार भागों में विभक्त वह रचना ही वेद है, ऐसा नहीं है. स्वयं इस वेद में ही ‘ नेति नेति’ कहकर छोड़ दिया गया है.

संस्थापक, आर्यकृष्टि वैदिक साधना विहार
वैदिक संस्कृति के अन्वेषक, लेखक, फिल्मकार
भू.पू. सीनियर प्रोड्यूसर एवं निर्देशक, ज़ी नेटवर्क
भू.पू. व्याख्याता ( भूगोल एवं पर्यावरण), मुम्बई
वेद अवश्य श्रुति है। पर क्या केवल वेद ही श्रुति है ?
ऋषयो मंत्रद्रष्टार: ……. ऋषियों ने मन्त्रों को देखा और उसे बैखरी वाणी में अभिव्यक्त किया। कहते हैं ये यह मन्त्र परमात्मा की प्रकृति के वे विधान है जिनका बोध एवं दर्शन ऋषियों ने किया था। धर्म यानि जिन नियमों ने प्रकृति को जन्म दिया है, जिसके आधार पर यह सृष्टि हुयी है. इसे विधि भी कहते हैं. विधि और विधाता अभेद हैं. इसे प्रकृति का विज्ञान भी कह लीजिये। इसी आधार पर ब्रह्माण्ड की, देवी -देवताओं, ग्रह -नक्षत्रों, आकाशगंगाओं, निहारिकाओं, सप्त लोकों और अनगिनत लोकों सहित पृथ्वी पर जीवों कि रचना हुयी है. पेड़, पौधे, आकाश, वायु, पशु पक्षी सहित मनुष्य की रचना हुयी। जो अस्तित्व यानि जीवन को और उसके वर्द्धन को धारण करता है. इसीलिए धर्म मनुष्य का बनाया नहीं है. यह मनुष्य -निर्मित नहीं है. इसीलिए वेद ‘अपौरुषेय’ कहा जाता है.
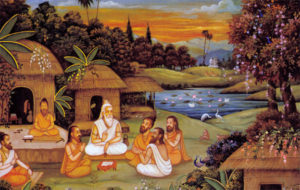
जब मनुष्य अस्तित्व में आया तो उसने सीखना शुरू किया कि कैसे उसका जीवन सुरक्षित रहे और कैसे विकास और विवर्द्धन हो. यह दोनों tendencies सभी प्राणियों में, जड़ -चेतन सब में अंतर्निहित है. पृथ्वी पर मनुष्य अलग -अलग समुदायों की अलग -अलग सभ्यताएँ हुईं। अलग -अलग भौगोलिक परिस्थति रही. सबने अपने -अपने ढंग से धर्म को यानि प्रकृति को, प्रकृति की कोशिश शुरू की. ताकि जीवन बेहतर हो सके. उनमें से एक सभ्यता हुई आर्यों की. आर्य सभ्यता के ज्ञानियों ने प्रकृति के mechanism का जो बोध किया, दर्शन किया उसे अपनी भाषा में व्यक्त किया। इस बोध को, इस जानने को ही ‘वेद’ कहा गया. उन्होंने कहा कि वे जो कह रहे हैं उसके निर्माता वे नहीं हैं बल्कि जो उन्हें दर्शन हो रहा है उसे ही बस अपनी भाषा में pass on कर दे रहे हैं. इसलिए उन ज्ञानियों ने अपने को उसका रचनाकार होने का दावा नहीं किया, बल्कि सिर्फ द्रष्टा कहा. जो धर्म है यानि जो प्रकृति का mechanism है, विज्ञान है. वह खुद तो कुछ बोल नहीं सकता। उससे हम बातें नहीं कर सकते। उनकी जानकारी सिर्फ उनको जानने वाले से ही मिल सकती है. हवा अपने आप नहीं बताता । अतः धर्म अथवा विधि अथवा विधाता ( abstract idea ) को जब तक कोई मनुष्य व्यक्त न करे तब तक मनुष्य को हो सकती। वेद भी मनुष्यों द्वारा ही व्यक्त हुए. ज्ञानी जनों ने साधना से उसे देखा।
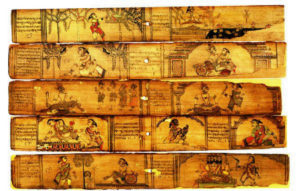
अब सवाल यह उठता है कि किस पद्धति से उन्होंने मन्त्रों का दर्शन किया, इन मंत्रद्रष्टा ऋषि-गण की बातें क्यों मानी जाएँ, कौन-से बड़े पहुँचे थे की सब सही समझ पाए, किसने देखा है की उन्होंने जो देखा वह सही देखा या त्रुटी रह गयी, किस युग में उन्होंने यह सब व्यक्त किया, उस युग के पहले लोग सत्य कैसे समझ पाते थे ? स्मृतिकार भी ऋषि थे, मंत्रद्रष्टा ऋषि ने भी स्मृति से ही यह सब कहा, फिर दोनों में फर्क क्या है, यदि श्रुति है तो कौन बोल रहा था, यह कैसे मान लिया गया की कोई था ही !!
वेद सदा है इसका अर्थ यह नहीं है की जिस रूप में बैखरी में अभिव्यक्त हुआ है उसी रूप में !!! बल्कि इसका भाव है कि उसमें निहित जो ज्ञान है वह सनातन है, वह ऋषियों द्वारा अभिव्यक्त होने के पहले भी था। बैखरी वह वाक् है जिसमें जीवों द्वारा उच्चारित सभी वाक् आते हैं. [ वाक् की उत्पत्ति उस समय ( अथवा उस स्तर पर )की है जब पदार्थ की सृष्टि भी नहीं थी (है). सबसे पहले परा वाक् उत्पन्न होता है। परा वाक् घनीभूत होकर पश्यन्ती का रूप लेता है जो घनीभूत होकर मध्यमा वाक् का. यह वह वाक् है जिसका प्रयोग हम सोचने में करते हैं. यह मध्यमा वाक् जब घनीभूत होकर जीवों के मुख से निकलता है तो वह बैखरी वाक् कहलाता है. अब मध्यमा के प्रत्येक वाक् के लिए बैखरी वाक् नहीं है। इसलिये मन मे सोचा सबकुछ हम भाषा मे बोल के अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अन्य तरीकों का सहारा लेते हैं। रो कर, हँस कर, मुस्कुरा कर, body expressions से, नाच कर, कूद कर, गीत से, संगीत से, नाट्य से, आजकल स्माइली से भी या नाना प्रकारों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृत से ! मध्यमा के ऊपरी वाक् में मानवीय भाषाएँ नहीं हैं। पश्यन्ति का अनुभव और प्रयोग के लिए चेतना को मिनिमम सविकल्प समाधि अवस्था में होना होगा और उससे ऊपर जो परा वाक् है उसके लिए निर्विकल्प समाधि और उसके ऊपर की अवस्था अनिर्वचनीय है। आज तक किसी भाषा में उसका प्राकटय नहीं हुआ है। ऋषयो मन्त्रद्रष्टार: ! ……………… जो ऋषि है वही मन्त्र का दर्शन कर सकता है. ऋषि होने के लिए कम से कम निर्विकल्प / सविकल्प समाधि तक तो पहुँचे ही होंगे तब जाकर परा एवं पश्यन्ति वाक् स्वरुप में प्रकृति के mechanism का दर्शन हुआ होगा, बोध हुआ होगा….. उसके बाद ही उस ज्ञान को उन्होंने बैखरी में ऋचाओं के रूप में व्यक्त किया हो वेद कहलाया।
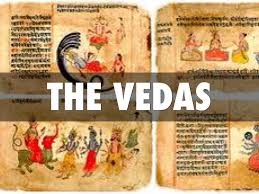
इस तरह, एक तो धर्म / विधि जिसको हम विधाता भी कहते हैं. वह एक कल्पना है जिसके स्वरुप की कोई थाह हमें नहीं है. अपने-अपने हिसाब से सबके ख्याल हैं. दूसरे वे कुछ व्यक्ति जिन्हे परमपुरुष कहते हैं जिन्हे सभी ऋषियों ने परमपुरुष माना है और धर्म का एकमात्र वक्ता कहा है. परमपुरुष की उक्तियाँ श्रुति हैं. परमपुरुष वो शक्ति हैं जिसे हम विधाता कहते हैं और अपने निराकार रूप में सदा सर्वव्याप्त हैं. जब वे सदेह मानव रूप में प्रगट होते हैं तो धर्म को परिस्थितियों और तत्कालीन चुनौतियों के अनुसार explain करते हैं. आम जनता उन्हें आम रूप में ही समझती है पर कुछ limited ज्ञानी जन उनके वास्तविक रूप का दर्शन कर पाते हैं.
जो ज्ञानी हैं, ऋषि, महर्षि, मुनि, वैज्ञानिक हैं वे परमपुरुष द्वारा बताये गए मार्ग पर चलते हैं. उसे और विस्तार से समझाते हैं, व्याख्या करते हैं, guide करते हैं. ये लोग किताबें लिखते हैं जिन्हे शास्त्र कहते हैं. परन्तु जो १००% perfection परमपुरुष में होता है वह उनमे नहीं होता इसलिए उनके शास्त्रों को स्मृति आदि का दर्जा दिया जाता है. स्मृति आदि जबतक श्रुति-सम्मत हैं तब तक मान्य हैं. साक्षात परमपुरुष श्रीकृष्ण एवं श्रीराम जैसे साक्षात परमपुरुष जो अपने श्रीमुख से अभिव्यक्त करते हैं वह भी तो परम श्रुति है। इनमे तो वेदों से भी उच्च कोटि का ज्ञान है। :– ” त्रैगुण्य-विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन !” (- गीता २- ४५ में श्रीकृष्ण) ” वेदों में तीन गुणो के ही विषय हैं. तुम इन तीनो गुणों का त्याग करो अर्थात वेद से उपर उठो, हे अर्जुन।
अतः श्रीराम एवं श्रीकृष्ण जैसे परमपुरुष की जो -जो डायरेक्ट वाणियाँ ( स्वयं कही हुयी) वे सब परम श्रुति ही हैं. वेद की ऋचाएँ तो ऋषियों ने देखी हैं। ऋषियों की तुलना में स्वयं ईश्वर की अभिव्यक्ति ही मान्य होगी।
वेद के मन्त्र द्रष्टा ऋषियों ने जो देखा वह व्यक्त किया. हम *”मान”* कर चलते हैं कि कोई ‘निराकार’ ने वह सब कहा है। कब कहा ? कैसे कहा ? ऋषियों ने जो दिव्यज्ञान से बोध किया वही न ?! इसकी तुलना में परमब्रह्म परमपुरुष जो साक्षात अभिव्यक्त कर हैं वह तो अविवादित रूप से सर्व श्रेष्ठ है। वेद जिनके बारे में बताने की हैं कोशिश कर रहे हैं और नेति- नेति कहकर बतला पाने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, स्वयम उस अव्यय, अच्युत परमेश्वर की ही कही हुयी बात सर्वोपरि मानी जायेगी। इसमें कोई guess नहीं. इसमें सब ज्ञात है। ऋषि-मुनि साधक हैं, फाइनल अथॉरिटी नहीं। सिर्फ अवतीर्ण परमपुरुष ही फाइनल अथॉरिटी होते हैं. धर्म के वक्ता सिर्फ परमपुरुष ही होते हैं. उनमे १००% परफेक्शन होता है. भ्रान्ति या गलती होती ही नहीं. जैसे – राम एवं कृष्ण।
ऋषि मुनि आदि जो लोग साधना कर के भाँति-भाँति के उच्च स्तरों का दर्शन करते हैं, बोध प्राप्त करते हैं वे साधक लोग ऋषि, मुनि, संत, महात्मा होते हैं पर पुरुषोत्तम अवतीर्ण होते हैं. ब्रह्म के साकार रूप. ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह जन्म से ही होते हैं. उनमे ह्रास विकास नहीं होता। वे सदा पूर्ण होते हैं. इसलिए ऐसे नरदेही परमपुरुष ही फाइनल ऑथरिटी हैं. ब्रह्म का एक निराकार रूप है जो एक कल्पना है। जो ब्रह्म सामने मनुष्य रूप धर कर पुरुषोत्तम के रूप में सामने खडा है वह सामने यथार्थ है। …जो सर्व शक्तिशाली परमतत्व परमपुरुष के रूप में कह रहा है उस से ऊपर भला और क्या हो सकता है !
मनुस्मृति में मनु कहते हैं – ‘श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय:” आदिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभि: सर्वा: सत्यविद्या: श्रूयन्ते सा श्रुति:॥‘ वेदकालीन महातपा सत्पुरुषों ने समाधि में जो महाज्ञान प्राप्त किया और जिसे जगत के आध्यात्मिक अभ्युदय के लिये प्रकट भी किया, उस महाज्ञान को ‘श्रुति’ कहते हैं।
चौदह मनुओं के जो सृष्टिकर्ता हैं उन ब्रह्मा जैसे असंख्य ब्रह्माओं की सृष्टि करने वाले परमपुरुष तो उनसे बहुत ऊपर के स्तर के हुए यह स्पष्ट है !!! हम सभी जानते हैं कि समस्त वेद गायत्री में समाहित हैं। गायत्री को वेदगर्भा कहा जाता है। गायत्री की उत्पत्ति शिव से कही जाती है। वे ही ओंकार के प्राणपुरुष हैं। इसीलिए वेदों में मात्र त्रिगुणात्मक जगत का वर्णन ही मिलता है और उसके ऊपर थोड़ा -बहुत इंगित पाया जाता । वे ब्रह्मा-विष्णु-महेश की त्रिधारा से नीचे के लोकों का ही वर्णन करते हैं। इसीलिये इनमें विष्णु की भी अधिक चर्चा नहीं मिलती। प्रत्येक ब्रहांड के अपने ब्रह्मा-विष्णु एवं महेश हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड परमपुरुष में स्थित हैं। ……. महर्षि वेदव्यास ने विष्णु सहस्रनाम में जो परमपुरुष श्रीकृष्ण के बारे में कहा है वह सबको पढ़ना चाहिए। गीता में भी श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा है की वेद मात्र त्रिगुणात्मक जगत का ही ज्ञान देते हैं। गुणातीत पुरुषोत्तम परमपुरुष के बारे में उनमें क्या मिलेगा !

वेद वे श्रुति हैं जिन्हें ऋषियों ने बताया. उन्होंने कहा की उन्होंने ये सब देखा है, खुद नहीं सृजित किया….[ मैं समस्त पुराणों एवं स्मृतियों के बारे में बात नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ उन्ही अंशों / parts के बारे में कह रहा हूँ जो परमपुरुष की डायरेक्ट उक्तियाँ हैं। ].इस प्रकार हम देखते हैं कि परमपुरुष की उक्तियों में वेदों से बहुत ही ऊपर के स्तरों का ज्ञान है, इसमें संदेह नहीं। अतः निस्संदेह परमपुरुष की उक्तियाँ परम श्रुति हैं। अन्यथा फिर यह मानना पडेगा की ब्रह्म के स्वयं कहे हुए से फलाँ -फलाँ ऋषि का कहा श्रेष्ठ है !! यह तो संभव ही नहीं।
परमपुरुष के मनुष्य -रूप में प्रगट होने पर उन्हें ‘परमपुरुष’ के रूप में कैसे पहचाना जाता है ? उस लीलाधर की माया अत्यंत दुष्कर होती है।
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥१०- २॥ – गीता में श्रीकृष्ण [ ” न मेरे आदि (आरम्भ) को देवता लोग जानते हैं और न ही महान् ऋषि जन क्योंकि मैं ही सभी देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ।” [ द्रष्टव्य:- सभी वेद पुराण एवं शास्त्र महर्षियों द्वारा ही रचित हैं.]
अवजानन्ति मां मूढ़ां मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्॥९- ११॥
[ इस मानुषी तन का आश्रय लेने पर (मानव रुप में अभिव्यक्त करने पर), जो मूर्ख हैं वे मुझे नहीं पहचानते। मेरे परम भाव को न जानते कि मैं इन सभी भूतों का (संसार और प्राणीयों का) महान् ईश्वर हूँ।]
एकमात्र अनन्य भक्ति और प्रेम से ही वे अपने स्वरुप को उस भक्त के सामने प्रगट करते हैं। विरले ऋषि तपस्वी एवं भक्त उन्हें पहचान पाते हैं. गीता में प्रभु कहते हैं :– ” मेरे इस रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है इस रूप को न वेदों के अध्यन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिये, तत्व से जानने के लिये तथा प्रवेश करने के लिये अर्थात् एकाकार हो कर प्राप्त होने के लिये संभव हू। हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है- वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है । ” (11:53-55)