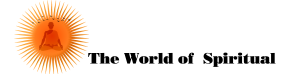कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् |
जीवन में जितनी संपत्ति बढ़ती है उतना खालीपन भी बढ़ता है। आज आधुनिक मानव की सुविधाओं का स्तर बढ़ गया है । पर क्या मानव सुखी हुआ है ? क्या जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है ? जीवन की गुणवत्ता ही वास्तविक जीवन स्तर है। आज का जीवन व्यस्त है अर्थात कर्म अधिक है । विराम और विश्राम, दोनों ही कम है। ऐसे में कर्म को सुव्यवस्थित करने का विज्ञान व उसमें आनन्द लेने की कला, दोनों जानना अत्यावश्यक है। भगवद्गीता के सभी अध्यायों को योग का सम्बोधन मिला है। यहाँ तक की अर्जुन के रोने को भी अर्जुनविषादयोग कहा है क्योंकि गीता हमें कर्म का विज्ञान व कला दोनों सीखाती है। यह अत्यन्त व्यावहारिक उपदेश है। योग के अर्थ को जानने में अष्टांग योग के बाद इस कर्मयोग को समझने का यत्न करते है।

गीता में योग की तीन चार परिभाषायें आती हैं। एक है ‘‘योगः समाधि!’’ अपने अधिष्ठान को सम्यक कर लेना ही योग है। अधिष्ठान यानी नीव, जिसपर हम स्वयं को निर्भर पाते है। बालक का अधिष्ठान उसके अभिभावक होते हैं। वह पूर्ण निर्भय होकर कर्म करता है। उसे पता रहता है कि माँ सम्हाल लेगी। पड़ोसी के बच्चें से निःसंकोच लड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि पिता रक्षा करेंगे। तनाव और चिंता तब प्रारम्भ होती है जब हम अपने अहं में अपने कर्म का अधिष्ठान कर लेते है। तब सारी जिम्मेवारी ही अपनी हो जाती है और फिर यदि कर्म का प्रशिक्षण नहीं है तो फिर ये जिम्मेवारी व्यक्ति को कुचल देती है। आधुनिक महत्वाकांक्षी मानव की यही समस्या है। अधिष्ठान को सम्यक करने का तात्पर्य है ऐसी नीव बनालो कि हमारे कर्म निर्भय हो जाये। भक्तिमार्गी कहेंगे ईश्वर पर अधिष्ठान कर लो। राजयोग अपने अधिष्ठान को, मन के आधार को संतुलित करने की बात करता है। यह मन के अभ्यास द्वारा भी सम्भव है। भक्ति में मन के समर्पण द्वारा भी और ज्ञान मार्ग में परम् ज्ञान के द्वारा स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने पर भी सम्भव है। ‘रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते’ विषयों के रस में रमनेवाली प्रज्ञा परम सत्ता के दर्शन से ही रसों से मुक्त होती है। सारी कामनाये नष्ट हो जाती है – ‘प्रजहाती यदा कामान्’ और अधिष्ठान अपने आप में स्थित हो जाती है – ‘आत्मैव आत्मना तुष्टः’। यह सम्यक अधिष्ठान है किसी पर निर्भर नहीं है। कर्मयोग में भी अधिष्ठान को सम्यक करने की विधि बताई है। यहाँ अधिष्ठान को ही निरर्थक बना दिया जाता है। इसी से हम गीता में योग की दूसरी परिभाषा पर आते है।
दूसरी परिभाषा है ‘‘योगः कर्मसु कौशलम्’’। कर्म को योगयुक्त बुद्धि से करना ही कुशलता है। यह तो कुशलता की परिभाषा है। इसमें योग तो उपकरण है। योग में रत बुद्धि से किया कर्म। इसी कारण दूसरे अध्याय के इस भाग में इसे बुद्धियोग कहा है। सांख्ययोग के अनुरुप बात बताने के बाद 39 श्लोक में भगवान् कहते अब बुद्धियोग सुन। इसी को व्याख्याकारों ने कर्मयोग भी कहा है। इस पूरे विवरण में ही यह व्याख्या आती है। कई बार कर्म में कुशलता योग है ऐसा अर्थ बताया जाता है किन्तु जब हम पूरे श्लोक को देखते है तो सन्दर्भ के साथ बात स्पष्ट होती है। पूरा श्लोक है-
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते।
तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम।। 2.50।।
प्रथम पंक्ति में बताया है ‘बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते’। बुद्धि से युक्त होने से कर्म के बन्धन फिर चाहे वह सुकृत, अच्छे हो या दृष्कृत, बुरे सब नष्ट हो जाते है। जल जाते है। कैसी बुद्धि? योग की बुद्धि। दूसरे अध्याय के ही 41 वे श्लोक में भगवान इस योगयुक्त बुद्धि की परिभाषा बताते है। ‘व्यवसायात्मिका बुद्धिः ऐकेह कुरुनन्दन’। लक्ष्यप्रेरित जीवन जीने वाला व्यक्ति व्यावसायिकता का परिचय देते हुए अपनी बुद्धि को लक्ष्य पर एकाग्र करता है। जो बहुविध बातों में अपनी बुद्धि को शाखाओं में बाँटता है वह अव्यावसायिक है। इससे अधिक व्यवावहारिक सिद्धान्त क्या होगा? लक्ष्यप्रेरित बुद्धि, एकाग्र बुद्धि को ही कृष्ण भगवान् योग से परिपूर्ण अर्थात युक्त-बुद्धि कह रहे है। ऐसी युक्त-बुद्धि को पाने के लिये योग में रत हो जाओ। अर्जुन के माध्यम से हम सब को कह रहे है ‘तस्मात योगाय युज्यस्व’ इसलिये योग से जुड़ जाओ। आचरण में लाओ। ‘योगः कर्मसु कौशलम’ यही कुशलता से कर्म करने का मार्ग है। ‘कर्मसु योगः’ का अर्थ है योग युक्त कर्म। यह कर्मयोग का रहस्य है। इसी से हम गीता में वर्णित योग की तीसरी परिभाषा पर आते है।
तीसरी परिभाषा है ‘‘समत्वं योग उच्चते’’। मन को समत्व की स्थिति में रखना अर्थात अनुकुल या प्रतिकुल प्रत्येक स्थिति में मन समता में रहें। कर्मयोग में लक्ष्य पर एकाग्र बुद्धि के बाद दूसरी अनिवार्यता है संग का त्याग। संग अर्थात चिपकना। जब हम आसक्ती के साथ कर्म करते है तब अपेक्षाओं के दुष्चक्र में फँसते है। अपेक्षा पूर्ण होने या ना होने पर हमारा आनन्द निर्भर रहता है। इससे हम कर्म में आनन्द नहीं ले पाते। कर्म में ध्यान ही नहीं लगा पायेंगे। ध्यान तो सतत परिणाम पर ही जायेगा। इसलिये संग का त्याग करों। क्यों? इसका विज्ञान पूर्व के श्लोक में समझाया। बड़ा ख्यात श्लोक है किन्तु उतना ही विभ्रम का भी कारण है ।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।।2.47।।
हमारा अधिकार केवल कर्म पर ही है – ‘कर्मणि एव अधिकारस्ते’ । वहीं हम पूर्णता से कर सकते है। ‘मा फलेषु कदाचन’ फल पर कभी भी हमारा अधिकार नहीं है। यह उपदेश नहीं है। यह जीवन के सत्य का मात्र विधान है, कथन है। फल में तो कई कारक है। गीता ही अन्य एक जगह कर्म और सिद्धि के पाँच कारक बताती है। पहला है साधन, करणं (Instruments, Tools), दूसरा कारणं अर्थात उद्देश्य (Purpose), तीसरा कर्ता (Doer), चौथा अधिष्ठान (Foundation) और पाँचवा दैव (Fate) । पहले तीन कारकों पर हमारा अधिकार है। चौथे के बारे में हमने उपर देखा है। जब पहले तीन को युक्त बुद्धि व संग रहित होकर सर्वश्रेष्ठ (Perfect) कर लिया तो अधिष्ठान उस प्रक्रिया में ही निहित हो जाता है, उसका अलग से महत्व समाप्त हो जाता है। कर्मयोग अधिष्ठान को निरापद बना देता है और ऐसे सम्यक अधि-समाधि को प्राप्त करता है। पाँचवें पर तो हमारा कोई बस नहीं है। अतः फल पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरी पंक्ति में उपदेश या निर्देश है। इसलिये तू फल का हेतु मत बन क्योंकि तेरा अधिकार नहीं है और आलस के संग में भी मत फँस क्योंकि कर्म पर तेरा पूरा अधिकार है। हमने बड़ी सहजता से इतनी सुन्दर प्रक्रिया का विपर्याय कर दिया ‘कर्म करो फल की चिंता मत करो।’ यह नहीं हो सकता। लक्ष्य तय करो। उस पर ध्यान केन्द्रित कर पूरे योग से कुशल कर्म करों। फल का हेतु मत बनों।
लेकिन कैसे? तो श्रीकृष्ण ने उसकी विधि बताई –
योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भुत्वा समत्वं योग उच्चते।। 2.48।।
योग में स्थित होकर कर्म करों। संग का त्याग करों। कैसे त्याग करों? सिद्धि और असिद्धि दोनों मे सम रहकर। हमारे पूर्ण कुशल कर्म के बाद सफलता और असफलता दोनों को समान निरपेक्षता से स्वीकार करना संग का त्याग है। यह समत्व ही योग कहलाता है। इन तीनों सुत्रों को एकसाथ जीवन में उतारने से कर्मयोग व्यवहार में उतरेगा। पूरा जीवन ही आनन्दमय हो जायेगा। यही कर्म का रहस्य है, उसको समझने का विज्ञान भी और उसको करने की कला भी।